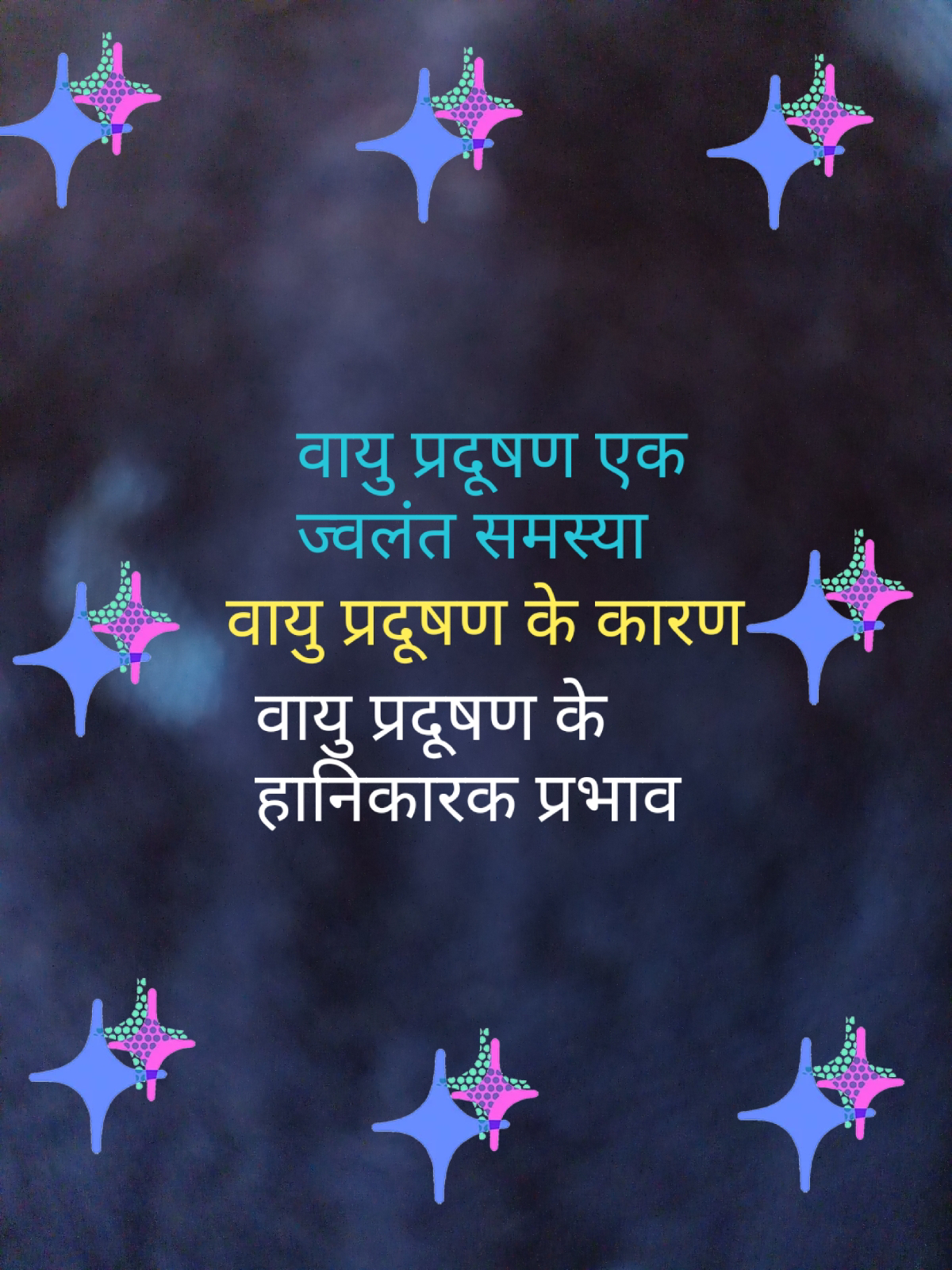माँ ममता की मूरत ही तो है इस बात को मानने से कभी कोई इन्कार नहीं कर सकता।माँ एक शब्द मात्र नहीं है बल्कि एक एहसास है।माँ शब्द ही ऐसा है , जिसे किसी परिभाषा के दायरे में नहीं बाँधा जा सकता और न ही माँ के प्यार को अहसान माना जा सकता है ।माँ अनगिनत भावनाओं का पुंज है , जो मन के आँगन में बरबस छलक पड़ता है ।
माँ स्वयं ही एक उत्सव है , उसका होना ही उत्सव है।मातृत्व ही तो माँ का आभूषण है।माँ होगी तो मातृत्व होगा और मातृत्व में माँ समाहित होती है ।पश्चिमी देशों की तुलना में हमारा देश अत्यन्त सौभाग्यशाली है कि हमारी संस्कृति मातृत्व प्रधान संस्कृति है, जहाँ माँ ही सर्वोपरि है ।ममता एवं मातृत्व के उत्सवों में विकसित हुई हमारी मातृत्व प्रधान संस्कृति में माँ होना एक बहुत बड़ा सम्मान है।
माँ तप, त्याग, समर्पण एवं बलिदान का जीवंत प्रतीक है।उसके आँचल में बचपन पोषित होता है, यौवन समृद्ध होता है और जीवन नई ऊँचाइयों को छूता है।माँ के सजल स्पर्श से जीवन सदा पुलकित रहता है।माँ के बिना जीवन अनाथ हो जाता है।माँ ही तो है "परमात्मा"।हमारी पूजा-पाठ की अवधारणा तो माँ के बिना अधूरी है।बंगाल में छोटी-छोटी लड़कियों को माँ कहकर पुकारना हमारी मातृप्रधान संस्कृति का प्रतीक है।
कभी हम अचानक किसी संकट में फँस जाएँ, तो सबसे पहले हमारे मुख से माँ शब्द ही निकलता है।बच्चों की परवरिश में माता जो स्नेह बच्चों पर लुटाती है , जितना उनका ध्यान रखती है, इस कारण बच्चों को सदा माँ की ही जरूरत अधिक होती है।हालाँकि बच्चों के सर्वांगीण विकास में माता-पिता दोनों की ही समान भूमिका होती है ।
एक माँ जो भी अपने बच्चों के लिए करती है, उसे कोई और नहीं कर सकता, इसलिए अक्सर ही सुनने में आता है कि माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता ।माँ के लिए यदि संभव हो तो वह अपने बच्चों के लिए आसमान से तारे तोड़कर ले आए और चाँद को जमीन पर उतार दे , कहने का तात्पर्य है कि माँ अपने बच्चों को खुश रखने की हर संभव कोशिश करती है। इसीलिए इस पूरी दुनिया में माँ से ज्यादा अपने बच्चों को प्यार करने वाला कोई दूसरा नहीं होता ।
हमारी संस्कृति में चाची-ताई के रिश्ते भी छोटी माँ, बड़ी माँ जैसे प्यार भरे संबोधन में रचे-बसे हैं ।नानी माँ, दादी माँ जैसे संबोधन भी हमारे पास हैं ।ममता की इसी शीतल छाँव में हमारा जीवन तृप्त, तुष्ट एवं पुष्ट होता है। असीम प्यार एवं अंतहीन ममता के आँचल में हर मनुष्य का जीवन विकसित होता है।इसीलिए तो माँ को गर्भरूपी ममता की कोख मिली है।माँ के अलावा यह किसी के पास नहीं होती और हो भी नहीं सकती । कभी-कभी किन्हीं परिस्थितियों के कारण बच्चों की परवरिश माँ के बिना भी होती है।
वर्तमान समय में अधिकांश महिलाएँ कामकाजी हैं वे बाहर के एवं घर के काम-काज को निभाने , इनके बीच सामंजस्य बैठाने के प्रयास में कहीं न कहीं अपने बच्चों चाहकर भी को पूरा समय नहीं दे पा रही हैं ।फिर भी उनकी कोशिश रहती है कि बच्चों की परवरिश में कोई कमी न हो।
दौर चाहे जो भी हो , माँ की जगह बच्चों के लिए कभी नहीं बदली और नही कभी बदल सकती है।माँ की परम अनुभूति में जगन्माता की झलक दिखती है।जब किसी बच्चे को छोटी सी चोट लग जाए तो वह बिलखकर अपनी माँ के आँचल में छिप जाता है।दुख-दर्द की अनगिनत घटनाओं के समय बच्चे माँ की छाँव में पनाह लेकर सुरक्षित हो जाते हैं ।
ममता के कारण ही तो माँ है ।इसी ममता की छाँव तले माँ अपनी संतान में प्रारंभ से संस्कारों का बीजारोपण कर सके तो उन संस्कारों का बच्चे के जीवन में पुष्पित-पल्लवित होना सुनिश्चित है।इस तथ्य से सभी माताओं को परिचित होना चाहिए ।
समय की रेखा पर बहुत कुछ भूल जाते हैं लेकिन समय के साथ कोई जीवंत एवं चैतन्य होती जाती है तो वह है-- माँ की ममता।माँ के स्नेहिल स्मरण से हृदय भर आता है।माँ की यादें मेघ बनकर अंतःकरण में उमड़ती- घुमड़ती हैं ।माँ की ममता ने तो अपना सर्वस्व लुटा दिया है, उस ममता का मूल्य तो नहीं चुकाया जा सकता, परंतु माँ को आदर-सम्मान एवं प्रतिष्ठा देकर उस ऋण को कुछ हल्का किया जा सकता है ।
<<<<< मनोविज्ञान के अनुसार बच्चों पर माँ का प्रभाव >>>>>
भारतीय मनोविज्ञान के अध्ययनों के अनुसार--- माँ और बच्चे का रिश्ता कई विरोधाभासों के बाद भी उम्र के एक पड़ाव पर आकर एक हो जाता है ।मनोवैज्ञानिक यह भी कहते हैं--- भावनात्मक संबंधों के कारण ही माँ और बेटी के बीच कोई अंतर नजर नहीं आता है।इसलिए एक कहावत भी प्रचलन में है-- कि तुम तो अपनी माँ पर गई हो।मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि--- माँ का प्रभाव संतानों के चेतन, अवचेतन तथा अचेतन सभी पर पड़ता है ।विशेषकर अचेतन में माँ बस जाती है और वही अचेतन धीरे-धीरे संतान को उसकी माँ के जैसा गढ़ने लगता है।
माँ तो है ही ऐसी , जो हमें गढ़ती है , हमारे व्यक्तित्व में चार-चाँद लगाती है। ममता कभी कोई भेद नहीं करती --- बेटा-बेटी में अंतर नहीं करती , माँ तो सदा असीम होकर अनंत प्यार लुटाती है।
" माँ "
सादर अभिवादन व धन्यवाद ।